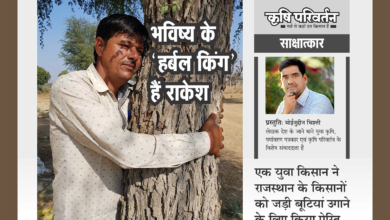हरियाणा के ही एक और किसान वैज्ञानिक हैं धर्मवीर कंबोज। इनकी भी जीवन-यात्रा रोचकता से भरी हुई है, जिसके हर पन्ने पर संघर्ष की दास्तान लिखी हुई है। इनके संघर्ष के दिन भी कम नहीं थे। घड़ी बेचकर दिल्ली आने का जुगाड़ बिठाया। फिर पुरानी दिल्ली में 16 से 18 घंटे तक रिक्शा चलाया। 1987 में एक एक्सीडेंट में रिक्शा टूट गया और चोट लगी सो अलग। साल 2008 में इनकी मासिक आय मात्र 4000 रुपये थी।
पर अब हालात कुछ और हैं, सन 2014 में वे राष्ट्रपति भवन में किसान वैज्ञानिक के तौर पर 20 दिन तक मेहमान रह चुके हैं जहाँ उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग मशीनों से खजूर, गुलाब, चेरी, अमरूद, जामुन आदि के उत्पाद बनाकर दिखाए।

वे अब प्रोसेसिंग की मशीनें बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी एक मशीन को 1,71,000 रुपये में खरीदा गया। अब तक 200 से ज़्यादा मशीनें देश-विदेश में बेच चुके हैं। 2013 में इन्होंने 75 लाख रुपये की मशीनें बेचीं, जिससे इन्हें 20 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। 2014 में सवा करोड़ की मशीनें बेचीं। यह ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।
धर्मवीर जी की भावी योजना है कि वे ग्वारपाठे का कैप्सूल बनाएँ। उनकी तमन्ना यह भी है कि भारत के सभी जिलों में उनकी बनाई मशीनों के शोरूम खुलें। उनका बेटा प्रिंस अब पढ़-लिखकर उनके काम-काज को युवा गति से आगे बढ़ा रहा है।
सम्पर्क: गांव व पोस्ट दामला,
जिला यमुनानगर (हरियाणा)
पिन कोड-135001
ईमेल: [email protected]
मोबाइल: 09896054925