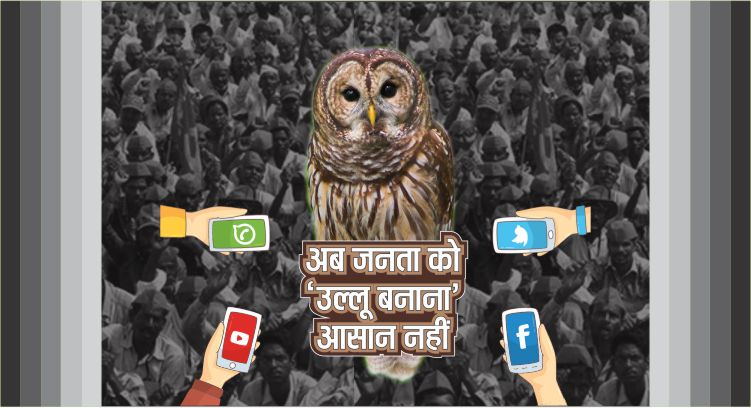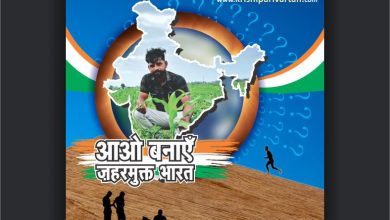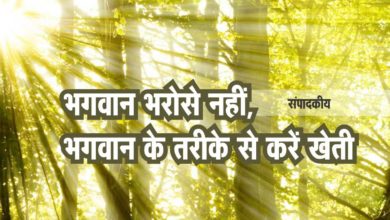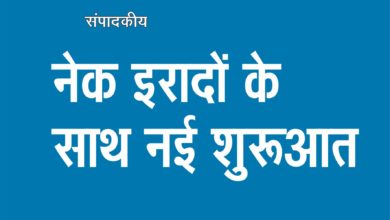वर्तमान समय में जब दुनिया तकनीकी और आर्थिक प्रगति की नई ऊँचाइयाँ छू रही है, तब एक गहरा और असहज प्रश्न हमारे सामने खड़ा है—क्या हमारा भविष्य ज़हरमुक्त होगा? यह प्रश्न केवल हवा, पानी या भोजन में फैले रासायनिक ज़हर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी तत्वों की ओर इशारा करता है जो आज हमारे जीवन, समाज, और विचारों को दूषित कर रहे हैं। इनमें पर्यावरणीय असंतुलन, मानसिक विषाक्तता, सामाजिक भेदभाव, भ्रष्टाचार और लालच; सभी शामिल हैं।
पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु संकट: ज़हर हमारे चारों ओर…
आज पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हमारे लिए सबसे बड़े वैश्विक खतरे बन चुके हैं। औद्योगीकरण, वनों की कटाई, वाहनों की बढ़ती संख्या और कोयले व तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा परिणाम है ग्लोबल वॉर्मिंग, बढ़ती गर्मी की लहरें, बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा या सूखा, और समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि।
जलवायु परिवर्तन एक अदृश्य ज़हर है जो धीरे-धीरे हमारे प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा को नष्ट कर रहा है। यह बच्चों, बुज़ुर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध हो रहा है। क्या हम इस ओर आँखें मूँदकर आगे बढ़ सकते हैं?
विचारों और समाज में फैलता मानसिक ज़हर…
एक और बड़ा संकट है — हमारी सोच और समाज में घुलता विष। आज व्यक्ति अपने ही समाज से कटता जा रहा है। धर्म, जाति, भाषा और राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर लोगों को बाँटा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जो कभी संवाद और जानकारी के साधन माने जाते थे, अब झूठ, नफ़रत और ध्रुवीकरण का अड्डा बनते जा रहे हैं।
यह मानसिक ज़हर धीरे-धीरे समाज को खोखला कर रहा है। बच्चों में आक्रोश, युवाओं में अवसाद, और वयस्कों में तनाव बढ़ रहा है। हमें शिक्षा प्रणाली, मीडिया और पारिवारिक मूल्यों को दोबारा मानवता, सहिष्णुता और सत्यनिष्ठा की ओर मोड़ना होगा।
राजनीतिक और आर्थिक विष: जब नीति में नैतिकता मर जाती है…
भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होते हैं। जब निर्णय जनहित की बजाय निजी स्वार्थ पर आधारित हों, तो समाज विषाक्त हो जाता है। बढ़ती बेरोज़गारी, अमीर-गरीब की खाई और कॉरपोरेट का नियंत्रण, यह सब आर्थिक विष के उदाहरण हैं।
हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, और आम आदमी के हित में हो। जब तक राजनीति और नीति निर्माण में नैतिकता नहीं आएगी, तब तक ज़हर केवल बढ़ता रहेगा—भले ही दिखाई दे अथवा नहीं।
रसायन-मुक्त खेती: ज़हर के ख़िलाफ़ एक सशक्त कदम…
हमारे भोजन की थाली में जो अनाज, फल और सब्जियाँ आती हैं, वे अब पहले की तरह शुद्ध नहीं रहीं। रासायनिक खाद, कीटनाशक, और हार्मोनल स्प्रे से उगाई गई फसलें न केवल मिट्टी और जलस्रोतों को दूषित कर रही हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हैं। इससे कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, मानसिक रोग और प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसे गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं।
जैविक या प्राकृतिक खेती (Organic or Natural Farming) इस संकट का समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें:
• गोबर खाद, कम्पोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है।
• मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
• भूजल प्रदूषित नहीं होता।
• किसान को दीर्घकालिक लाभ मिलता है।
सरकारें अब धीरे-धीरे जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन इसे एक आन्दोलन बनाना होगा। जब उपभोक्ता खुद जैविक उत्पाद माँगेंगे, तब किसान भी इस दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। हमें खपत की संस्कृति को बदलना होगा—‘सस्ता’ नहीं, ‘स्वस्थ’ सबसे ज़रूरी होना चाहिए।
उम्मीदें: क्या सबकुछ नकारात्मक ही है?
बिलकुल नहीं। अंधकार में भी आशा की किरणें हैं। बदलाव की लहरें शुरू हो चुकी हैं। युवा पीढ़ी पहले से अधिक जागरूक है। वे पर्यावरण की चिंता करते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर मुखर हो रहे हैं। स्कूलों में ‘टिकाऊ विकास (सस्टेनेबल डिवेलपमेंट),’ ‘हरित ऊर्जा,’ ‘अधिकाधिक वस्तुओं के अधिकाधिक पुनः उपयोग,’ ‘प्लास्टिक मुक्त जीवन,’ ‘लैंगिक समानता’, ‘मानसिक स्वास्थ्य’ और ‘सामाजिक न्याय’ जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। कई किसान जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। लोग स्वस्थ जीवन-शैली, मेडिटेशन और पर्यावरण- संवेदनशीलता को अपना रहे हैं। इन छोटे-छोटे प्रयासों को अगर हम एक सामूहिक जनांदोलन बना दें, तो निश्चित ही हम एक ज़हरमुक्त भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग यदि सही दिशा में हो, तो बदलाव संभव है।
हमारा भविष्य ज़हरमुक्त हो सकता है, लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी होगी; प्रकृति से लेकर विचारों तक, हर स्तर पर शुद्धिकरण ज़रूरी है। हमें विकास की परिभाषा को फिर से गढ़ना होगा—जहाँ लाभ से ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात हो, और विज्ञान के साथ संवेदनशीलता भी हो। यदि हम आज ज़हर से लड़ने का संकल्प लें, तो आने वाला कल न केवल ज़हरमुक्त, बल्कि समृद्ध और सुंदर भी हो सकता है। भविष्य ज़हरमुक्त हो सकता है, लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। इसके लिए हमें आज ही यह तय करना होगा कि हम कैसी दुनिया अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं:
• एक दमघोंटू, गर्म और विषैली धरती?
• या एक हरियाली, शांति और समरसता से भरा जीवन?
यदि हम जलवायु को संतुलित करने, रसायन-मुक्त खेती को अपनाने, विचारों को साफ़ और नीति को नैतिक बनाने की दिशा में अभी से कदम उठाएँ तो न केवल हमारा, बल्कि सम्पूर्ण मानवता का भविष्य सच में ज़हरमुक्त हो सकता है।
जिनके विचार शुद्ध हैं, उनका पर्यावरण भी शुद्ध होगा — और वही ज़हरमुक्त कल रचेगा।
पवन नागर
www.krishiparivartan.com
Youtube Handle: @krishiparivartan2013